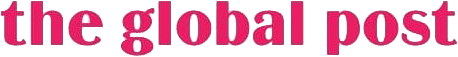लाइफस्टाइलस्वास्थ्य
मलेरिया का जानलेवा डंक, कारण और बचाव

मलेरिया खून की एक बीमारी है जो प्लाजमोडियम पैरासाइट के कारण होती है. यह एक खास तरीके के मच्छर के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है. यह गंभीर बीमारी है, कभीकभी यह बहुत घातक साबित होती है. यह एक ऐसे संक्रमित मच्छर के काटने से पैदा होती है जो अपनी लार में मलेरिया पैरासाइट को ले कर चलता है.
यह पूरी तरह रोकथाम और इलाज योग्य मच्छरजनित बीमारी है. मलेरिया के संदिग्ध रोगी का इलाज जल्द से जल्द मैडिकल निगरानी में किया जाना चाहिए. अगर किसी में मलेरिया की पुष्टि होती है तो उस का इलाज बहुत जरूरी है. सामान्य तौर पर इस का इलाज किसी अयोग्य व्यक्ति से नहीं कराया जाना चाहिए. कभी भी मलेरिया होने पर ओझा, गुनिया, तांत्रिक या भगतों के पास न जाएं. इलाज के दौरान दवाएं बीच में छोड़ना खतरनाक हो सकता है. इस के अलावा खाली पेट मलेरिया की दवाएं नहीं खानी चाहिए.
मलेरिया पैरासाइट एक सूक्ष्म जीव है जिसे प्लाजमोडियम के नाम से जाना जाता है और यह प्रोटोजोन्स के नाम से जाने जाने वाले छोटे जीवों के एक समूह से जुड़ा है. मच्छर की वह प्रजाति जो मलेरिया पैरासाइट को ढोने का काम करती है, एनोफिलीज कहलाती है. इसे मलेरिया वेक्टर्स कहा जाता है. यह एनोफिलीज मच्छर खासकर सुबह व शाम के वक्त काटता है. बरसात के मौसम के दौरान और उस के ठीक बाद यह चरम पर होता है. यह उस समय भी पैदा हो सकता है जब कम प्रतिरोधक क्षमता के लोग मलेरिया के फैलाव वाले सघन क्षेत्रों में जाते हैं.
मलेरिया एक तेज बुखार वाला रोग है. संक्रमित मच्छर के काटने के बाद एक गैरप्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान में इस के लक्षण 7 दिनों के बाद या फिर उस से ज्यादा (आमतौर पर 10 से 15 दिन) दिनों में जाहिर होते हैं. इस में बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, थकान और उल्टी हो सकती है लेकिन मलेरिया के तौर पर इस की पहचान कर पाना मुश्किल हो सकता है. मलेरिया से ग्रसित लोग अकसर फ्लू की बीमारी का अनुभव करते हैं. गंभीर मलेरिया से ग्रसित बच्चे में एक के बाद एक ये लक्षण जल्दीजल्दी आते हैं. गंभीर एनीमिया, पाचन अम्लरक्तता के चलते श्वसन तंत्र में तनाव या फिर सेरिब्रल मलेरिया. अगर 24 घंटे के भीतर इस का इलाज नहीं हो पाया तो गंभीर संकट पैदा हो सकता है. यह गंभीर बीमारी अकसर मौत का कारण बन जाती है.
कैसे फैलता है मलेरिया
जब मच्छर किसी इंसान की त्वचा से खून चूसता है तो ये परजीवी शरीर में दाखिल हो जाते हैं और फिर ये परजीवी लिवर में पहुंच जाते हैं और वहां ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और 8-10 दिन बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंच कर तेजी से हमला कर संख्या भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं.
काटने से बचने के उपाय
-
ऐसी जगहों पर खड़े हों जहां दरवाजों व खिड़कियों पर स्क्रीनिंग हो. अगर यह संभव नहीं है तो इस बात को सुनिश्चित करें कि दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हैं.
-
एक ऐसी मच्छरदानी के नीचे सोएं जिस को कीटनाशक के साथ धोया गया हो.
-
नींद के समय अपनी त्वचा पर कीट से बचाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें.
-
हाफपैंट की जगह ढीलेढाले लंबे पतलून और लंबी आस्तीन की शर्ट पहनें. खासकर शाम को और रात में ऐसा करें जब मच्छर भोजन करना पसंद करते हैं.
-
अवरुद्ध गटर और सड़क की नालियों को साफ कर मच्छरों की आबादी को कम किया जा सकता है. इस के अलावा, अपने यार्ड को पानी के खड़े कंटेनरों से मुक्त रखें.
-
कचरा, टिन, बोतलें, बालटी या फिर घरों के चारों ओर बिखरा हुआ कोई भी पदार्थ हटा कर उसे लैंडफिल में डाल दिया जाना चाहिए.
-
कारखानों और गोदामों में पैदा स्क्रैप सामग्री को हटाए जाने तक उचित तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए.
-
मच्छरों को मारने की दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए.